विकास का भ्रम: जनभागीदारी या दिखावा?
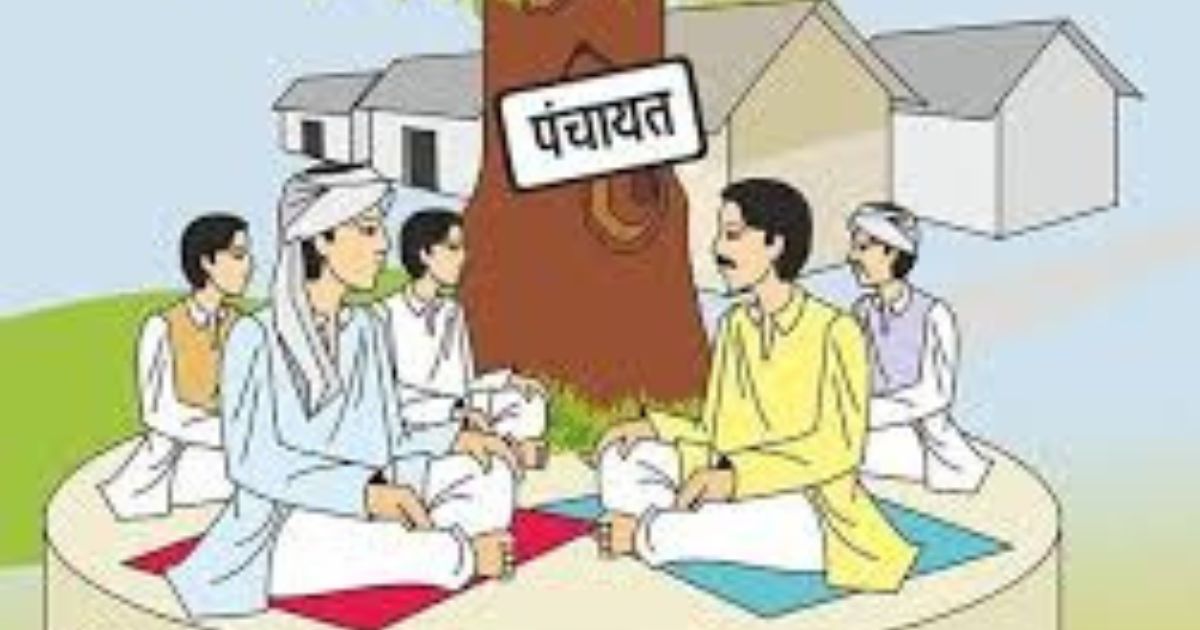
– देवेंद्र कुमार बुडाकोटी
उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की गहमागहमी अब थम चुकी है। उम्मीद की जाती है कि नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अब ग्रामीण विकास की गंभीर प्रक्रिया में जुटेंगे।
यह प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से सहभागी होनी चाहिए — ग्राम सभा की भागीदारी पर आधारित, जिसमें हर वयस्क ग्रामीण की आवाज़ शामिल हो। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है।
चुनाव के समय गांव का परिदृश्य एक मेले में तब्दील हो जाता है — जहां भोजन, शराब और वादों की भरमार होती है। प्रवासी लोग शहरों से लौटते हैं — कई बार उम्मीदवारों के खर्च पर — ताकि हर वोट सुनिश्चित हो सके।
लेकिन मतगणना समाप्त होते ही यह चहल-पहल गायब हो जाती है। जो लोग लंबी यात्रा करके वोट देने आए थे, वही लोग विकास की बैठकों से नदारद रहते हैं।
विकास योजनाओं की प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह जाती है — कागज़ भरे जाते हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन लोगों की वास्तविक भागीदारी कहीं गुम हो जाती है।
आज भी गांवों में वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है — ऊपर से थोपे गए सरकारी योजनाएं, जिन्हें “टॉप-डाउन अप्रोच” कहा जाता है। पंचायत प्रतिनिधि योजना निर्माण में शामिल नहीं होते, फिर भी उन्हें दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं।
इस व्यवस्था की जड़ें 1952 में शुरू हुए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम (CDP) में मिलती हैं। यह एक समग्र विकास की महत्वाकांक्षी पहल थी, जिसने एक विस्तृत नौकरशाही तंत्र को जन्म दिया।
जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO), ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO), और ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक, जिसे अब ग्राम विकास अधिकारी (VDO) कहा जाता है। लेकिन केवल पदों के नाम बदलने से गांवों की हालत नहीं बदली।
1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की — जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई।
फिर भी, 1980 के दशक में सरकार द्वारा कराई गई एक महत्वपूर्ण फील्ड स्टडी के नतीजे चौंकाने वाले थे। इसका दस्तावेज़ 1985 में प्रकाशित हुआ — “Grass Without Roots: Rural Development Under Government Auspices” — लेखक एल. सी. जैन और अन्य।
अध्ययन में पाया गया कि तीन दशकों की कोशिशों के बावजूद ग्रामीण गरीबी न केवल बनी रही, बल्कि कई मामलों में बढ़ी। यह रिपोर्ट सरकारी तंत्र की उस असफलता को उजागर करती है, जो जनता की ज़रूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने में अक्षम रहा।
1992 में लाया गया 73वां संविधान संशोधन इस व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने का प्रयास था — नियमित चुनाव, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण, और सबसे महत्वपूर्ण, सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रावधान। लेकिन जमीनी स्तर पर यह अभी भी अधूरा सपना बना हुआ है।
कोविड-19 महामारी ने इस विफलता को और उजागर कर दिया। लाखों प्रवासी — जो सामाजिक सुरक्षा से कटे हुए और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में फंसे थे — अपने गांवों को लौटे। यह रिवर्स माइग्रेशन देश की ग्रामीण-शहरी गतिशीलता की कमजोरी का प्रतीक बन गया। उत्तराखंड सरकार ने पुनर्वास योजनाएं घोषित कीं, लेकिन जैसे ही शहर खुले, अधिकांश लोग वापस लौट गए।
क्यों? क्योंकि योजना-निर्माण की प्रक्रिया में गांवों की आवाज़ शामिल नहीं थी। योजनाएं सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर अप्रासंगिक थीं। आज का ग्रामीण युवा — जो मोबाइल, सोशल मीडिया और शहरी चमक-दमक से प्रभावित है — अब उस ‘गांव’ को नहीं चाहता जो उसके दादा-दादी ने देखा था।
“ठंडो रे ठंडो, मेरा पहाड़ को पानी, ठंडी हवा” जैसी पंक्तियाँ बुज़ुर्गों के लिए भावुक हो सकती हैं, लेकिन यह आज की बेटी-ब्वारी को एक किलोमीटर चलकर पानी लाने के लिए प्रेरित नहीं करती। भावनाओं से मूलभूत सुविधाओं की कमी पूरी नहीं हो सकती।
अब समय आ गया है कि भारत सरकार, विशेष रूप से नीति आयोग, कुछ मूलभूत प्रश्न पूछे —
क्या हमें 1952 में बनी इस ऊपर-से-नीचे वाली मशीनरी को खत्म कर देना चाहिए?
जब तक राज्य केवल प्रतीकात्मक सहभागिता से आगे नहीं बढ़ेगा — और जनता पर विश्वास नहीं करेगा — तब तक हम विकास की घास तो उगाएंगे, पर उसकी जड़ें कभी नहीं जमेंगी।
लेखक एक समाजशास्त्री हैं, जो पिछले चार दशकों से विकास क्षेत्र में कार्यरत हैं।







